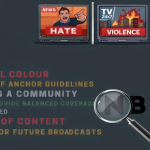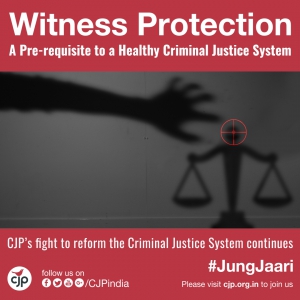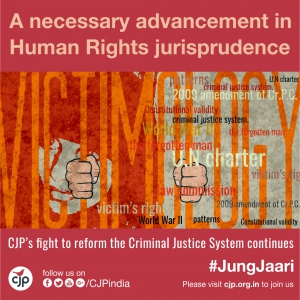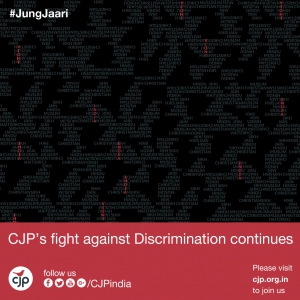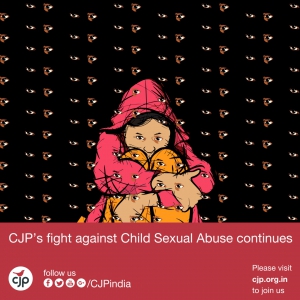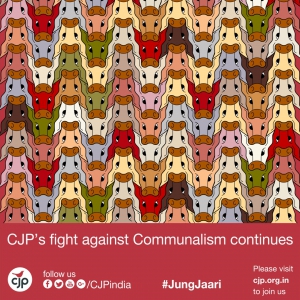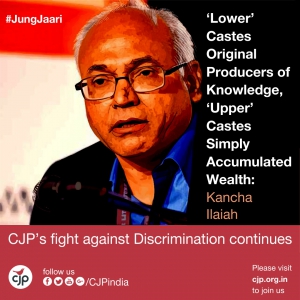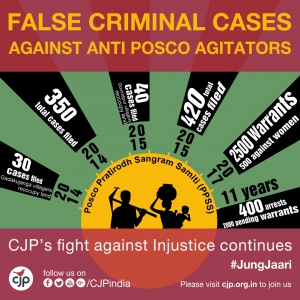कैसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 2023 में किए गए संशोधन, वन अधिकार अधिनियम, 2006 द्वारा आदिवासियों को दिए गए भूमि संरक्षण को कमजोर करने की कोशिश करते हैं: सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित वन (संरक्षण) अधिनियम, 2023 में किए गए व्यापक संशोधनों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा के साथ ही, आदिवासी और वन-निवासी समुदायों के अधिकारों पर पुनः एक गंभीर संकट मंडरा रहा है।
31, Oct 2025 | CJP Team
सर्वोच्च न्यायालय वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफआरए) और संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (एफसीए, 2023) के बीच के टकराव में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास पर विचार कर रहा है जो कि 2023 में एफसीए के विवादास्पद संशोधनों के बाद हुआ है। एफआरए 2006 का उद्देश्य आदिवासी और वनवासी समुदायों को निश्चितता और सुरक्षा देना था। यह दक्षिण एशिया और भारत के वनवासी समुदायों द्वारा वर्षों के आंदोलन के बाद लागू किया गया एक ऐतिहासिक कानून है। लेकिन मोदी सरकार के दौर में एफ़.सी.ए. (FCA) 2023 में बिना पर्याप्त संसदीय चर्चा के जो नई सरकारी शक्तियाँ और छूटें जोड़ी गईं, उन्होंने एक बार फिर भारत के आदिवासी समुदायों के लंबे संघर्ष से हासिल अधिकारों पर नया खतरा खड़ा कर दिया है। यह भारत की नीतियों के लिए एक अहम मोड़ है जहां हमें वन संरक्षण, आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नए नजरिए से समझने की जरूरत है।
वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 में लागू किया गया था। यह उन लोगों के लंबे संघर्ष का नतीजा था जो पीढ़ियों से जंगलों में रहते और काम करते आए हैं। इस कानून ने आदिवासी और स्थानीय लोगों को जमीन, घर और वनों के उपज (जैसे महुआ, तेंदू पत्ता, शहद आदि) पर हक दिया। साथ ही, ग्राम सभा को जंगल की देखभाल और प्रबंधन का अधिकार भी मिला। इसका मकसद था कि अब फैसले दिल्ली या वन विभाग नहीं, बल्कि गांव के लोग खुद करें। किसी भी जंगल की जमीन का इस्तेमाल बदलने से पहले ग्राम सभा की अनुमति जरूरी रखी गई। और यह माना गया कि विकेन्द्रीकरण ही जमीन के अधिकारों और जंगलों की सुरक्षा, दोनों के लिए सबसे जरूरी है।
वन (संरक्षण) अधिनियम, जो 1980 में लागू किया गया था – और 2023 में बिना किसी गंभीर बहस के जल्दबाजी में संशोधित कर दिया गया – शुरू से ही वन संरक्षण के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। 2023 के संशोधनों के बाद यह कानून और आगे बढ़कर वन भूमि पर केंद्रीकृत नियंत्रण को और मजबूत करता है। इन संशोधनों ने “वन” की परिभाषा को सीमित कर दिया और सुरक्षा व व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए व्यापक छूटें दे दीं। साथ ही, कानून के तहत पहले से की गई वन भूमि के इस्तेमाल में बदलाव (diversions) को नियमित करने की अनुमति भी दे दी गई। इन बदलावों ने समुदाय से परामर्श की प्रक्रिया खत्म कर दी, पर्यावरणीय सुरक्षा को कमजोर किया और अंततः विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी समुदायों की भूमि अधिग्रहण को आसान बना दिया। अब एफसीए (FCA) के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, वन भूमि को अन्य उपयोगों में बदलने (diversion) की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही ग्राम सभा की सहमति की शर्त को भी कमजोर कर दिया गया है – जिससे अब समुदाय से परामर्श महज़ एक औपचारिकता बनकर रह गया है।
इस समय यह याद करना बेहद जरूरी है कि फरवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी बेदखली आदेश ने पूरे देश में आदिवासी और वनवासी समुदायों के बीच बड़े और लंबे विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था। उस आदेश का उद्देश्य और असर इतना बड़ा था कि इससे करीब एक करोड़ वनवासी और आदिवासी लोग अपनी ज़मीन और घरों से उजाड़े जा सकते थे। इसलिए, यह आदेश भारत में भूमि और वन अधिकारों की लड़ाई का एक और महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसने आदिवासी और वन समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर संगठन और आंदोलन को जन्म दिया और देशभर में नागरिक समाज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी – जिनमें प्रमुख रूप से ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल्स (AIUFWP) और सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) शामिल थे। सिर्फ दो हफ्तों के भीतर, देशभर के नागरिक समाज संगठनों के दखल से – जिनकी ओर से लगभग डेढ़ दर्जन अंतरिम याचिकाएं दायर की गईं – सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बेदखली आदेश पर रोक लगा दी। यह कदम तब और जरूरी हो गया जब जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल कर मामले की दोबारा समीक्षा करने की अपील की।
यह मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और यह दर्शाता है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता और संरक्षण नीतियों के बीच संघर्ष अब भी जारी है। 24 अक्टूबर 2025 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय (MOTA) ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस याचिका का कड़े शब्दों में विरोध किया, जिसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत बनाए गए 2012 के नियमों की वैधता को चुनौती दी गई है। यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से सामने आई है। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने काउंटर एफिडएविट में, केंद्र सरकार ने न केवल इस कानून की कानूनी वैधता का बचाव किया है, बल्कि यह भी जोर देकर कहा है कि यह कानून सिर्फ जमीन के स्वामित्व को नियमित करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य जंगलों पर निर्भर समुदायों की गरिमा, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान को बहाल करना भी है।
एआईयूएफ़डब्ल्यूपी (AIUFWP) एक राष्ट्रीय स्तर की, महिलाओं के नेतृत्व वाली संगठनात्मक यूनियन है, जो वनवासियों, कृषि मजदूरों और आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है। यह संगठन स्थानीय समुदायों में नेतृत्व विकसित करता है, खासकर आदिवासी महिलाओं के बीच और समान न्याय (distributive justice) की वकालत करता है। साथ ही, यह पूरे भारत में विभिन्न संगठनों और हितधारकों के साथ मिलकर समुदाय आधारित पारंपरिक वन अधिकारों की कानूनी मान्यता और संरक्षण के लिए काम करता है। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण और कानूनी सहयोग देकर सीजेपी (CJP) एक कानूनी अधिकार और वकालत करने वाला संगठन है जो एआईयूएफ़डब्ल्यूपी (AIUFWP) के साथ मिलकर काम करता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विस्तृत अंतरिम याचिका (Interlocutory Application – IA) में, सीजेपी न केवल सह-याचिकाकर्ता (co-petitioner) थी, बल्कि उसने याचिका का मसौदा तैयार करने में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस अंतरिम याचिका (IA) में भारत के आदिवासी समुदायों के ऐतिहासिक रूप से उनके अधिकारों से वंचित रखे जाने का विस्तार से उल्लेख किया गया था – वही अन्याय, जिसने 2006 के वन अधिकार अधिनियम को जन्म दिया। याचिका में यह भी बताया गया कि कैसे दावों को व्यवस्थित रूप से खारिज किया गया, न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, ग्राम सभाओं की भूमिका को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और वन प्रशासन ने 2006 के कानून की मूल भावना और प्रावधानों का उल्लंघन किया।
आगे की सुनवाईयों में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने मूल आदेश से आगे बढ़ते हुए सभी राज्यों को हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इन हलफनामों में राज्यों से यह बताने को कहा गया कि उन्होंने वन अधिकार दावों की जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसे की और जिन दावों को पूरी तरह खारिज किया गया, उनके पीछे के कारण क्या थे। अब यह तय करना कि समुदाय को भूमि अधिकार सही तरीके से दिए गए हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों की कार्यवाही में कितनी पारदर्शिता को पर्याप्त मानती है।
इस महत्वपूर्ण मामले (वाइल्डलाइफ फर्स्ट, जिसमें आदिवासी यूनियनों और अन्य ने हस्तक्षेप किया है) के अलावा, उसी समय सर्वोच्च न्यायालय – एक अन्य पीठ – 2023 में जल्दबाजी में लागू किए गए वन (संरक्षण) अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती देने पर विचार कर रहा है, जो वैधानिक संरक्षण (एफआरए 2006 के तहत) और राज्य संप्रभुता (एफसीए के तहत) के बीच की खाई को चौड़ा करेगा। जैसा कि हाल ही में एक पीठ की टिप्पणियों में सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया गया है, सामूहिक बेदखली को रोकने का मुख्य आधार वन अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त भू-स्वामित्व और कल्याणकारी अधिकारों तथा वन (संरक्षण) अधिनियम द्वारा संरक्षण के लिए कथित रूप से लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के बीच अनसुलझे नीति और कानून विरोधाभास पर केंद्रित है। इस तरह, यह मामला भारत की दो जिम्मेदारियों के बीच फंसा है – एक तरफ जंगलों में रहने वाले लोगों के अधिकार, और दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण की जरूरत। इसी वजह से अधिकारों और नियमों के बीच टकराव पैदा हो गया है, जो आगे भी अदालतों में उठता रहेगा।
FCA संशोधनों की आलोचना खास तौर पर उत्तर-पूर्वी भारत पर उनके असर को लेकर की जा रही है, जहां बहुत से जंगलों को सरकार ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन वे वहां के आदिवासी और स्थानीय समुदायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन संशोधनों में ग्राम सभाओं की राय को महत्व नहीं दिया गया। इससे लोगों की भागीदारी घट गई है और अब “ग्रीन क्रेडिट” और एक ही किस्म के पेड़ लगाने की योजनाओं को लेकर लोगों में चिंता है। 1996 के गोडावरमन फैसले ने “वन” की परिभाषा को बढ़ाकर उसमें गैर-श्रेणीबद्ध (unclassified) और सामुदायिक (community) जंगलों को भी शामिल कर लिया था। लेकिन हाल ही में रद्द किए गए नए कानून में ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्रों को मान्यता नहीं दी गई है, जो अब शोषण और दोहन का शिकार हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का रुख साल दर साल बदलता रहा है। उदाहरण के तौर पर, वाइल्डलाइफ फर्स्ट मामले में एक अलग दिशा दिखाई दी थी जबकि बाद में नियमगिरी फैसले में अदालत ने यह माना कि जंगलों के इस्तेमाल या हस्तांतरण से पहले ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है। फिर भी, आदिवासी अधिकारों की कानूनी स्थिति इस समय अस्पष्ट और कुछ हद तक अनिश्चित है – खासकर जंगलों के इस्तेमाल को लेकर। अब फैसले लेने का अधिकार सरकारी विवेक पर ज्यादा निर्भर हो गया है, जिससे समुदायों के अधिकार और संवैधानिक गारंटियां पीछे छूटती नजर आती हैं।
वन प्रबंधन से आदिवासी समुदायों को बाहर रखना कोई नया चलन नहीं है- इसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल से हुई थी, जब कानूनों ने उन्हें जमीन और संसाधनों के रक्षक नहीं, बल्कि अतिक्रमणकारी (encroachers) के रूप में देखा था। वन अधिकार अधिनियम (FRA) को इस ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति और उसे सुधारने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन-निवासियों के भूमि, संसाधन और स्वशासन के अधिकारों को मान्यता देता है। वन अधिकार अधिनियम (FRA) दशकों तक चले अधिकार-आंदोलनों और समुदायों के निरंतर प्रयासों का बहुआयामी और सशक्त परिणाम था। इसने न केवल उनके जंगलों तक पहुंच और इस्तेमाल के अधिकारों को स्वीकार किया, बल्कि उनकी आजीविका की मान्यता, वन शासन के लोकतांत्रिकीकरण और वंचित समुदायों की गरिमा की पुनर्स्थापना की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम प्रस्तुत किया।
कई मायनों में, वन (संरक्षण) अधिनियम के जरिए केंद्रीकृत शासन के विस्तार को 1996 के सुप्रीम कोर्ट के गोडावरमन फैसले ने वैधता प्रदान की। यह एक महत्वपूर्ण मामला था जिसने “वन” की प्रशासनिक परिभाषा को बहुत हद तक विस्तारित कर दिया। केंद्रीकृत नियंत्रण की यह प्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) की मूल भावना के विपरीत है। यह अधिनियम वन प्रबंधन में विकेन्द्रीकरण और समुदाय-आधारित अधिकारों के एजेंडे को सशक्त आधार प्रदान करता है। यह तनाव केवल प्रशासनिक या प्रबंधकीय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वास्तविक और संवैधानिक रूप से स्थापित संघर्ष है जो कार्यपालिका (सरकार) और अधिकार-संपन्न ग्राम सभाओं के बीच शक्ति-संबंधों में दिखाई देता है। यही संघर्ष विकास, संरक्षण और आदिवासी अधिकारों के उद्देश्यों के बीच मौजूद मूलभूत टकराव को उजागर करता है।
गोडावरमन बनाम भारत संघ (1996) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा –
“‘वन’ शब्द का अर्थ उसके शब्दकोशीय अर्थ के अनुसार लिया जाना चाहिए। यह परिभाषा उन सभी विधिक रूप से स्वीकृत वनों को समाहित करती है – चाहे वे आरक्षित, संरक्षित या अन्य किसी श्रेणी के अंतर्गत क्यों न आते हों – वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2(1) के प्रयोजन के संदर्भ में। धारा 2 में प्रयुक्त ‘वन भूमि’ शब्द न केवल शब्दकोशीय अर्थ में समझे जाने वाले ‘वन’ को शामिल करेगा, बल्कि सरकार के अभिलेखों में दर्ज किसी भी ऐसे क्षेत्र को भी सम्मिलित करेगा जिसे वन के रूप में दर्ज किया गया हो – चाहे उसका स्वामित्व किसी के पास भी क्यों न हो।” (गोडावरमन बनाम भारत संघ, 1996) के विपरीत, वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 अपने विधिक उद्देश्यों को इस प्रकार स्थापित करता है – “वनों में पीढ़ियों से रह रहे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन-निवासी समुदायों के वन अधिकारों तथा वन भूमि पर उनके कब्जे को मान्यता प्रदान करना और उन्हें वैधानिक रूप से निहित करना; ताकि उन पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जा सके – क्योंकि ये समुदाय वन पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व और स्थायित्व के लिए बेहद आवश्यक और अभिन्न अंग हैं।”
2023 के वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधनों में “वन” की परिभाषा को पहले से अधिक सीमित कर दिया गया है और ग्राम सभाओं की भागीदारी के अवसर भी कम कर दिए गए हैं। यह बदलाव एक बार फिर कार्यपालिका (सरकारी तंत्र) के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में गया है, जिससे वन अधिकार अधिनियम (FRA) की विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता कमजोर पड़ गई है।
निष्कर्ष
मौजूदा परिस्थितियों में यह बेहद आवश्यक है कि एक पुनर्निर्मित और व्यापक नीतिगत ढांचा विकसित किया जाए, जो भूमि तथा साझा संसाधनों पर समुदायों के निहित एवं ऐतिहासिक अधिकारों को राज्य के उस एकपक्षीय दावे के साथ संतुलित कर सके, जिसके माध्यम से वह प्रायः कॉरपोरेट विकास के नाम पर भूमि का अधिग्रहण करता है। ऐसी जन-केंद्रित अधिकार व्यवस्था वह होगी जो संवैधानिक सुरक्षा-प्रावधानों का सम्मान करे, समुदाय-आधारित शासन प्रणाली को पुनर्स्थापित करे तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों की सार्थक भागीदारी को सुनिश्चित बनाए। भारत के वनों में हो रही लकड़ी की अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रण तभी संभव है जब सामुदायिक अधिकारों को पुनः स्थापित किया जाए और राज्य को उसकी संवैधानिक जवाबदेही के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाए। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप एक नई और संभावनापूर्ण शुरुआत का संकेत दे सकता है। भारत में वन संरक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब उन समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए जिन्होंने सदियों से इन वनों की देखभाल और संरक्षण किया है। इसके लिए जरूरी है कि ग्राम सभाओं की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया जाए, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और अधिकारों की मान्यता के लिए एक सुदृढ़ विधिक ढांचा विकसित किया जाए।
(CJP की विधिक अनुसंधान टीम में वकील और इंटर्न शामिल हैं; इस संसाधन पर उर्वी केहरी ने कार्य किया है।)
संदर्भ:
- India: Legacies and Challenges of the Land & Forest Rights Movement Booklet
- https://cjp.org.in/forest-conservation-amendment-act-2023-a-challenge-to-adivasi-land-rights-and-environmental-protections/
- https://cjp.org.in/what-is-the-forest-rights-act-2006-and-how-are-we-defending-it/
- https://cjp.org.in/sokalo-gond-and-nivada-rana-lead-the-campaign-for-forest-rights-in-sc/
- https://cjp.org.in/forest-rights-case-sc-directs-states-to-file-compliance-affidavits/
- https://cjp.org.in/forest-conservation-amendment-bill-north-east-to-bear-the-brunt/
- https://thewire.in/environment/the-forest-rights-act-and-the-battle-for-indias-forests
- https://www.scobserver.in/cases/constitutionality-of-the-frawildlife-first-v-ministry-of-forest-and-environment-eviction-of-forest-dwellers-background/
- https://www.sanctuarynaturefoundation.org/article/the-forest-%28conservation%29-amendment-act%2C-2023
- https://www.scobserver.in/journal/the-amended-green-law-is-full-of-red-flags-forests-amendment-act-2023/
- https://www.scobserver.in/reports/arguments-on-february-28th-2019/
- https://www.scobserver.in/reports/wildlife-first-v-ministry-of-forest-and-environment-eviction-of-forest0dwellers-arguments-on-september-12th-2019/
- Godavarman v UOI, 1996, Supreme Court of India