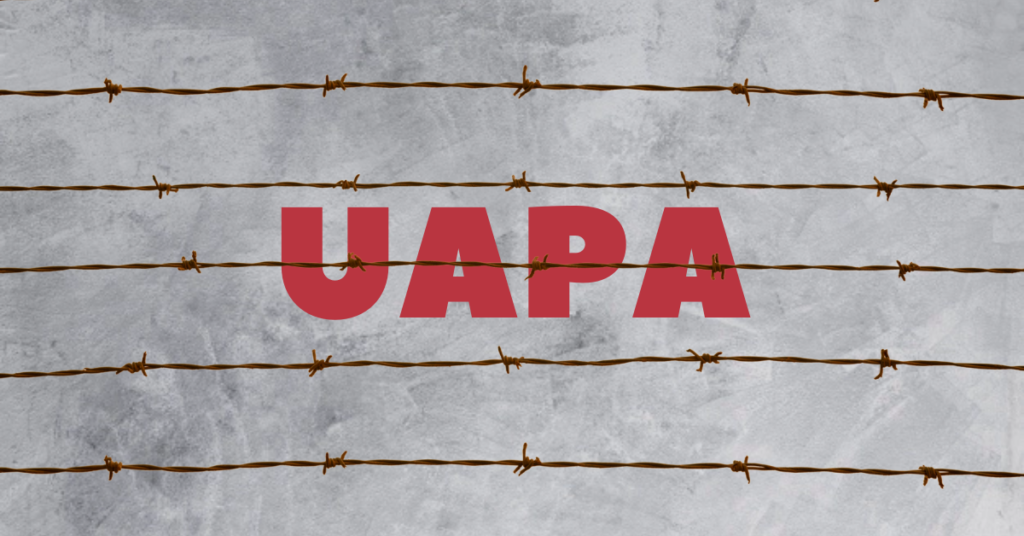कुछ ऐसे विनाशकारी लम्हे, जिनके होने की एक संभावना होती है। भले ही वे कुछ रूढ़ियों और अनसुलझे सवालों को पूरी तरह से नहीं बदलते हों पर कुछ ज़रूरी गुत्थियाँ खोलने और महत्वपूर्ण बदलावों के शुरुआत की वज़ह बन जाते हैं। दशकों से मानवाधिकार की रक्षा के लिए समर्पित चौरासी वर्षीय जेसुइट पुजारी फादर स्टेन स्वमी का हिरासत में मारा जाना, दरअसल एक ऐसी ही मौत है जो राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन.आई.ए) और महाराष्ट्र जेल अधिकारीयों का एक दुस्साहस भरा काम था। दोनों एजेंसियों के द्वारा की गई इस जघन्य कार्यवाही के बाद एक बार फिर से भारत के सभी गैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम को बारीकी से देखने और समझने कि जरूरत आन पड़ी है। 1960 में बने इस क़ानून में जिस तरह से जल्दबाजी में 2004, 2008, 2012 और 2019 में फेर बदल किया गया, जिसके चलते यह क़ानून आज भारत के सबसे ख़तरनाक आतंकवाद विरोधी क़ानून में तब्दील हो चुका है। जिसने न्यायशास्त्र की उस व्याख्या को ही बदल कर रख दिया है जिसे ‘असाधारण’ परिस्थितियों के लिए होना चाहिए अब उसे साधारण परिस्थितियों में लागू किया जा रहा है।
‘आतंक के अपराध’ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले 1980 के दशक में क़ानून लाया गया था। इसके बाद 2000 के दशक में इसी तरह का एक और क़ानून लाया गया। इसी के तहत सन् 1985 में पहली बार आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम 1985 को लाया गया था। जिसे बाद में कुछ फेरबदल करके आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1985 के रूप में संशोधित कर दिया गया। लेकिन 1995 में, जस्टिस जे.एस. वर्मा जो कि उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा संसद के सभी सदस्यों के बीच पत्र के माध्यम से अभियान चलाकर इस अधिनियम का पुरजोर विरोध किया गया था। जिसके कारण अंततः उस संशोधित अधिनियम को ख़ारिज करना पड़ा था। इस अभियान के दौरान चलायी गयी मुहिम में बताया गया था कि इस क़ानून के तहत दर्ज किए गए 76,000 मुकदमे का ‘राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद से जुड़े अपराधों’ से बहुत कम या कुछ भी लेना-देना नहीं है। उस दौरान पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात ने टाडा के तहत 20,000 मामले दर्ज किए थे। परन्तु उनमें से कोई भी मामला ऐसा नहीं था जिसका ‘आतंक के अपराध’ से कोई लेना-देना रहा हो। इस काले क़ानून का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ किया गया था। इसके तहत खासतौर से उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था जो सरकार की नीतियों (जीएटीटी (GATT) और डब्ल्यूटीओ (WTO) का विरोध कर रहे थे। इसके बाद दूसरा आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 में लाया गया। जिसे 2002 में संसद के संयुक्त सत्र के दौरान पोटा (POTA) के रूप में पारित कर दिया गया। इस क़ानून को पारित करने की जो मुख्य वजह बताई जाती है वह 1984 में हुआ एयर इंडिया जहाज का अपरहण और फिर 2001 में संसद पर हुआ हमला था। जिसने संसदीय आक्रोश को जन्म दिया था। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद उस समय की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA-I) सरकार द्वारा यूएपीए (UAPA -1967) को और भी ज़्यादा कठोर बनाने के लिए इसका दूसरा सेट लाया गया। इसका विरोध उस समय केवल सीपीआई, सीपीआईएम, ऐआईडीएमके, बीजेडी, और मीम ने किया था। हालाँकि, ‘आतंक’ को लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने के लिए इसे सामान्य आपराधिक क़ानून के दायरे में लाने की शुरुआत पहली बार सन् 2004 की गई थी। यह वही दिन था जब पोटा (POTA) को ख़त्म करने का चुनावी वादा भी पूरा किया गया था। हालाँकि यह सच है कि इन दोनों ही क़ानूनों (टाडा (TADA) और पोटा (POTA)) का इस्तेमाल चुनिंदा और लक्षित तरीके से किया गया। यानि इसका दुरुपयोग करते हुए इसे अंजाम दिया गया। इसके अलावा राज्य एवं क़ानून प्रवर्तन ने इसकी अलग-अलग व्याख्याएं करते हुए इसका इस्तेमाल उन अल्पसंख्यक समूहों के ख़िलाफ़ किया जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। मसलन, उन आदिवासियों और श्रमिकों के खिलाफ़ जो सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध कर रहे थे या फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना से पहले और बाद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस क़ानून के दुरुपयोग ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। पहली नज़र में लगता है कि भारत सरकार के द्वारा कोई नया दृष्टिकोण रखने के बजाय, यूएपीए (UAPA) 2004 और यूएपीए (UAPA) 2008 में भारी-भरकम संशोधन के लिए पुराने आतंकवाद विरोधी क़ानूनों के प्रावधानों से ही चीजों को व्यापक तौर पर शामिल कर लिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप यह क़ानून आज एक ऐसा सर्वव्यापी क़ानून है जो पुलिस/एजेंसियों को असीमित ताक़त देता है। जबकि लोगों के लिए कोई सुरक्षा या सुरक्षा उपायों के अधिकार को मुहैया नहीं कराता है। यकीनन, यूएपीए (UAPA) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20 (3), 21 और 22 का मौलिक रूप में उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह क़ानून मानवाधिकार अधिनियम, 1948 की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 10, 11, और 12; यूरोपीय मानवाधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 6; और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24-26 का भी उल्लंघन करता है।
आख़िर आतंक या आतंकवादी कारनामे को कौन किस तरह से व्याखित करता है और इस तरह के संगठित और पहले से तयशुदा हिंसा में इसकी व्याख्या किस तरह से फिट की जाएगी? संकीर्ण दायरे के कारण तथा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अभाव में यह काफी हद तक संभव है कि जिस आतंक को राजनीतिक समर्थन हासिल है वह न केवल क़ानूनी चंगुल से बच जाते हैं बल्कि इस बात की भी पूरी उम्मीद होती है कि वह बनाये जाल से भी बच निकलें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैरीलैंड जीटीडी (ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस), मैरीलैंड यूनिवर्सिटी, यूएस की ‘अपराधियों की विचारधारा पर आधारित भारत में आतंकवादी हमलों’ (terrorist attacks in India based on Ideology of Perpetrators) पर एक तुलनात्मक अध्ययन की रिपोर्ट से पता चलता है कि सन् 2004 से 2014 तक हुए कुल 5042 हमलों में से 42% हमले वामपंथी चरमपंथियों द्वारा, 22% अलगावादियों के द्वारा, 35% विविध या अज्ञात अतिवादियों के द्वारा अंजाम दिए गए। जबकि इस्लामिक चरमपंथियों के द्वारा इस तरह के बमुश्किल 1% के हमलों को अंजाम दिया गया था। यह संभावना है कि ‘विविध’ या ‘अज्ञात’ की श्रेणी में आने वाले हिंसक और चरमपंथी कारनामे को हिंदुत्व/हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता हो। यूएपीए (UAPA) की अनुसूची-1 में प्रतिबंधित संगठनों के रूप में 16+2 इस्लामिक संगठन; 15 अलगाववादी और अति वामपंथी संगठन को सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन मालेगांव बम ब्लास्ट (2006), हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट (2007), समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट (2007), अजमेर बम ब्लास्ट (2007), पनवेल बम ब्लास्ट (2008), ऑडिटोरियम बम ब्लास्ट (2012), मामलों में किसी भी संगठन को आरोपित नहीं किया गया। मॉब लिंचिंग और बड़े पैमाने पर जनता को लक्ष्य बनाकर आतंकित करने के अन्य मामलों के बारे में तो क्या ही कहा जाए। ऐसे संगठनों को न तो प्रतिबंधित ही किया गया है और न ही गैरक़ानूनी संगठन या आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।
इन क़ानूनों (जिसमे अब यूएपीए भी शामिल है) की कई विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि पुलिस अधिकारियों के सामने अपराध की स्वीकारता को साक्ष्य के रूप में मान्यता दे दी गयी है। यह एक ऐसा प्रावधान जो न केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का उल्लंघन करता है बल्कि जाँच के प्रावधान को भी ख़त्म कर देता है। यह यातना की खुली छूट देता है। इसके तहत आरोप लगने से पहले रिमांड के प्रावधान को बढ़ा कर 180 दिनों का कर दिया गया है। यहाँ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की वैधानिक और संवैधानिक जरूरत नहीं है। आरोप पत्र दाख़िल करने के लिए एजेंसी को दिया जाने वाला लंबा समय केवल व्यर्थ है। भारतीय आपराधिक क़ानून का सबसे मौलिक अधिकार, निर्दोष होने की संभावना होती है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20 और 22 के तहत रेखांकित किया गया है। परन्तु यह क़ानून आरोपी व्यक्ति को प्रभावी ढंग से आरोपों का मुक़ाबला करने या उससे पहले, यहाँ तक कि जमानत मिलने की संभावना को भी असंभव बना देता है। यूएपीए (UAPA) की धारा 43 डी (5) जमानत प्रावधानों को प्रतिबंधित करती है। किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर होने से पहले या फिर उसके बाद भी किसी भी तरह के जमानत की संभावना को ख़त्म कर देता है। यह प्रावधान, पहले टाडा (TADA) क़ानून की धारा 20 (8) और फिर पोटा (POTA) के धारा 49 (7) के तहत शामिल था। भारतीय आपराधिक क़ानून में मौजूद जमानत के प्रावधानों के बावजूद भी इस धारा के तहत उस वक्त तक यूएपीए (UAPA) में जमानत मिलना असंभव है जब तक कि (अ) लोक अभियोजक को नहीं सुना जाता है और (ब) कोर्ट, केस डायरी के अवलोकन के बाद यह राय नहीं बना लेती है कि व्यक्ति के ख़िलाफ़ आरोप को मानने के लिए आधार, प्रथम दृष्टया सही है”। निश्चित ही, यह धारा भारतीय आपराधिक क़ानून को अपने सिर के बल लाकर खड़ा कर देती है। अप्रैल 2019 में इस धारा को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली के मामले में अस्थिर न्यायिक के अनुमोदन से नवाजा गया है। इस मामले में अदालत का यह आदेश कि जबतक अदालतें प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में लगाये गए सभी आरोप को स्पष्ट न कर लें तबतक आरोपी को पूरे मुक़दमे के दौरान हिरासत में ही रखना चाहिये। इस पूरी कवायद ने जमानत के लिए गढ़े गए सिद्धांत पर प्रतिकूल असर डाला है।
दुनिया भर में आतंकवादी हमलों से पैदा हुई परिस्थितियों के परिणामस्वरूप राज्य (कार्यकारी और विधायिका) के द्वारा क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों को बेलगाम शक्तियां देने वाले क़ानूनों को पारित करने के लिए अक्सर आक्रामक उपाय अपनाया जाता रहा है। समय-समय पर जाँच और संतुलन (Check and Balance) के द्वारा परीक्षण किए गए उपायों और प्रक्रियाओं को रोकना सत्ता का दुरुपयोग है। भारत भी इससे अछूता देश नहीं है। बल्कि दूसरे उदारवादी लोकतंत्र भी इसी तरह के क़ानून को पारित कर चुके हैं। जैसे यूएसए ने ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप में कठोर क़ानूनों का गैर-क़ानूनी दुरुपयोग किया और कनाडा, यूनाइटेड किंग्डम और ऑस्ट्रेलिया में भी सनसेट क्लॉज़ (sunset clause) जैसे कुछ इस तरह के क़ानून बने हुए हैं। इस क़ानून के तहत कभी भी जरूरत पड़ने पर पारित हुए क़ानून को निरस्त करने का भी प्रावधान मौजूद है। इस क़ानून के तहत दर्ज मामलों की न्यायिक या संसदीय समीक्षा के लिए अंतर्निहित प्रावधान भी हैं। जबकि पोटा (POTA) क़ानून के तहत पोटा (POTA) समीक्षा समिति का प्रावधान था, लेकिन संशोधित यूएपीए (UAPA) इनमें से किसी भी समीक्षा या परीक्षण की इजाज़त नहीं देता। पोटा (POTA) के अंतर्गत सरकार के द्वारा संचालित समीक्षा कमेटी का प्रावधान था कि कमेटी पोटा (POTA) के अंतर्गत आने वाले सभी रजिस्टर्ड मामलों की समीक्षा 20 सितंबर 2005 तक पूरा करेगी। पोटा (POTA) समीक्षा कमेटी ने जून 2005 में जानकारी दी कि पोटा (POTA) क़ानून के तहत 11,384 लोगों पर ग़लत तरीके से आरोप लगाया गया था। उसके अनुसार ऐसे लोगों को पोटा के बजाय नियमित क़ानूनों के तहत आरोपित किया जाना चाहिये था।
यूएपीए (UAPA) का 2008 का संशोधन मोटे तौर पर आतंकवाद की व्याख्या पुराने वाले पोटा से भी बदतर करता है। 2008 के संशोधन के अनुसार “आतंकवादी अधिनियम” की परिभाषा वस्तुतः पोटा (POTA) प्रावधान के तरह ही है, जिसका एक खंड इसमें दुरुपयोग की पूरी गुंजाइश देता है। “(अ) भौतिक तत्व (एक्टस रीस) : एक आतंकवादी कृत्य वह है जिसमें “बम, डायनामाइट अथवा अन्य किस्म के विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ अथवा आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार का होना या फिर जहरीली अथवा हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या किसी अन्य पदार्थ का पाया जाना शामिल हो। ऐसा कुछ भी जिसे किसी ख़तरनाक उद्देश्य या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है” (जोड़ा गया)। इस जोड़े गए अंतिम वाक्या में समस्या है। क्योंकि यह मानता है कि किसी भी तरह फिजिकल/भौतिक काम एक आतंकवादी कार्यवाही हो सकती है। ऐसे में, यदि सरकार हल्के-फुल्के या थोड़ा-बहुत कोई सबूत लाकर अदालत को संतुष्ट कर देती, तो ऐसे में यह अधिनियम लोगों में डर पैदा करने का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत के सफाई कर्मचारी विरोध शुरू कर देते हैं तो यह तर्क दिया जा सकता है कि वे एक आतंकवादी कृत्य कर रहे हैं। क्योंकि हड़ताल से “ऐसे लोगों में डर पैदा होने की संभावना है”; जिनके पास आपातकालीन सहायता तक पहुँचने की सीमित पहुंच होगी। इस तरह से “किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके”, हड़ताल को” समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में व्यवधान डालने के रूप में देखा जा सकता है” तब हड़ताल धारा 15 की व्याख्या को संतुष्ट करने का कारण बन सकती है। यह सिर्फ एक उदाहरण है जोकि संशोधित यूएपीए (UAPA) के तहत आतंकवाद की परिभाषा को व्यापक तौर पर अस्वीकार्य बनाती है। पहले से ही स्थापित कठोर और क्रूर क़ानून को 2019 में एक बार फिर से संशोधन के जरिये और भी बदतर बना दिया गया। इस नए संशोधन को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया। इस तरह से केंद्रीय एजेंसी को सशक्त या हथियार बनाकर भारत के संघीय ढांचे को कमजोर किया गया और नुकसान पहुँचाया गया। हालाँकि एनआईए (NIA) के अधिनियम में 2019 के इस संशोधन से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालतों द्वारा दिए जाने वाले गुफ्तगू करने के आदेश के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। इससे भी बदतर यूएपीए (UAPA) के वे मामले है जिन्हें एनआईए (NIA) ने ‘अपने कब्जे में ले लिया’। ऐसे मामले सार्वजनिक जाँच के दायरे में अब नहीं हैं। अनुसूची VII, सूची II, प्रविष्टि 2 के अनुसार, क़ानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इस नाते भारतीय राज्य और समाज के संघीय ढांचे की तबाही के तौर पर इसे उदाहरण के बतौर देखा जा सकता है। धारा 6 (6) के तहत यदि केंद्र को ठीक लगता है तो वह राज्य सरकार को किसी भी विशेष मामले में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को एजेंसी को देने के लिए कह सकता है और राज्य मशीनरी द्वारा की जा रही जाँच को रोकने की भी मांग कर सकता है। दिल्ली की सीमाओं के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों को एनआईए (NIA) द्वारा जारी सम्मन, एनआईए के दुरुपयोग का हलिया उदाहरण है। मानव तस्करी, जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री, साइबर क्राइम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम- 1908 के तहत होने वाले अपराध एनएआई की सुपुर्दगी में देखे जाते हैं। जबकि मूल रूप से, एनआईए की अनुसूची में परमाणु ऊर्जा अधिनियम और गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 ही शामिल था।
हमने दिल्ली के साथ-साथ यूपी और असम में भी देखा कि असंवैधानिक नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 का विरोध करने वाले युवा छात्र नेताओं पर किस तरह से यूएपीए (UAPA) के तहत 23 मामलें दर्ज किये गए। यह एक निंदनीय कृत्य था। दिल्ली के अंदर यूएपीए (UAPA) के तहत बंद किये लोगों में से तीन ही अभी जमानत पर बाहर आ पाए हैं। हाल ही में, राज्बोर दल से निर्वाचित विधायक, अखिल गोगोई केपी यूएपीए (UAPA) के दो मामलों में बरी कर दिया गया है। ये ऐसे मामले हैं जो कि सार्वजनिक डोमेन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हजारों और भी मामले पड़े हुए हैं। जमानत पाने का महाकाय लक्ष्य केवल भीमा कोरेगांव के मामले या अखिल गोगोई के मामले तक ही सीमित नहीं है। बल्कि हाल ही में आंध्र-तेलंगाना से हुई गिरफ़्तारियाँ, हाथरस बलात्कार कांड, दिल्ली सीएए-एनआरसी के मामले, रिलायंस-श्रमिक मामले, झारखंड आदिवासी मामले में भी यह शर्मनाक रूप से स्पष्ट हो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि कई दूसरे मामलों में जैसे डॉक्टर बिनायक सेन, सोनोसोरी, सीमा आज़ाद, इमरान किरमानी, ग़ुलाम रसूल, एंजेला सोनटके और जियाउ रहमान और अन्य जाने-माने कार्यकर्ताओं के मामलों भी यह स्पष्ट हो चुका है कि दरअसल इन सभी को किसी आतंकवादी कृत्य में शामिल होने की वजह से जेल में नहीं रखा गया। बल्कि इन्हें यूएपीए (UAPA) के कठोर प्रावधानों के कारण ही लंबी अवधि तक जेल में रखा गया। 2017 में फादर स्टेन स्वामी ने भी झारखंड की जेलों में बंद पड़े करीब 4,000 आदिवासियों के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
अपनी सभी अंतर्निहित और कठोर शक्तियों के साथ, यह एक ऐसा क़ानून है जो न तो न्यायसंगत है, न पारदर्शी है और न ही जवाबदेह है और इसकी कोई एकरूपता भी नहीं है। इसे निरस्त करने के लिए इसमें सनसेट क्लॉज़ की न तो मौजूदगी है और न ही समीक्षा के लिए कोई प्रावधान है। जहाँ संप्रभुता लोगों के पास होती है ऐसे किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में मूल रूप से यह क़ानून किसी भी जरूरत को पूरा नहीं करता है। यह कोई न्यायसंगत क़ानून नहीं है। बल्कि यह एक हथियार है जिसका इस्तेमाल आतंक के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए नहीं बल्कि वर्तमान में भारत के लोगों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। यूएपीए (UAPA) नैसर्गिक न्याय को नकारने वाला महज क़ानून नहीं है, बल्कि यह क़ानून मौलिक स्वतंत्रता पर असंवैधानिक तरीके से अंकुश भी लगता है। आज़ादी के बाद, भारत ने समय-समय पर बहुत से क़ानून बनाये है : जैसे 1950 में निवारक निरोध अधिनियम, 1958 में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, 1972 में मीसा MISA (निरस्त), 1980 में एनएसए (NSA), 1990 में जम्मू-कश्मीर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे क़ानून बनाए गए। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्रीय सरकार को मात देने लिए राज्य सरकारों ने भी बढ़-चढ़कर बहुत से कठोर प्रावधानों के साथ क़ानून बनाये हैं- जैसे, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (1999), केसीओसीए (KCOCA) (2001), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम (2005) और गुजरात आतंकवाद तथा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (2019)। आरोप तय होने से पहले ही लम्बी अवधि तक कैदी बनाये रखना, इन क़ानूनों के इतिहास को और कलंकित करता है। यह एक तरह से दुरुपयोग की परंपरा है। आज़ादी से पहले आपराधिक क़ानून संशोधन अधिनियम 1908 था, जिसकी धारा 16 में स्पष्ट तौर लिखा गया था कि ब्रिटिश सरकार को किसी संगठन को गैरक़ानूनी घोषित करने और उसके सदस्यों को सजा देने की ताक़त हासिल थी। इस तरह से 1919 का अराजकतावादी क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, (रोलेट एक्ट) का इस्तेमाल, फैलते हुए राष्ट्रवाद को रोकने के लिए किया गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को वह शक्ति दी थी कि वह किसी को भी सरकार के ख़िलाफ़ साजिश करने या उसे उखाड़ फेंकने के संदेह में बिना मुक़दमा चलाये जेल में रख सकती थी। इस अधिनियम के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना उस पर कोई मुक़दमा चलाये दो साल तक कैद में रख सकती थी। क़ानून ने ऐसा अन्यायपूर्ण अधिकार दे रखा था। इसके बाद सशस्त्र बल विशेष अध्यादेश अधिनियम 1942 का इस्तेमाल ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ को रोकने के लिए किया गया। जिसके तहत सशस्त्र बल के चुनिंदा अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को पकड़ने और उसे ख़त्म करने का विशेष अधिकार हासिल था। आज यदि फादर स्टेन स्वामी की शहादत कोई वास्तविक बदलाव कर सकती है, तो उसे यह करना चाहिये कि देश में मौजूद राजनीतिक विपक्ष को इस उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के इतिहास को पूरी तरह से जवाब देने के लिए जागृत करना चाहिये। सीधी और सच्ची बात यह है कि 21वीं सदी के भारत में सत्ता या क़ानूनों के जरिये न्याय और समानता को आत्मसात करने की जरूरत है, न कि राज्य को अनियंत्रित सत्ता देने की।
जहाँ तक आकड़ों का सवाल है यह शासन किसी भी तरह के आकड़े को आमतौर पर सार्वजनिक नहीं करना चाहता है। हालाँकि, 9 मार्च, 2021 को लोकसभा में आयोजित एक प्रश्न के जवाब ने इस क्रूर क़ानून यूएपीए (UAPA) के तहत दर्ज मामलें और गिरफ़्तार किए गए लोगों के बारे में कुछ आंकड़े पेश किए गए। इन बताये गए आकड़ो के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 498 मामलें, मणिपुर में 386, तमिलनाडु में 308, जम्मू और कश्मीर में 227, झारखंड में 202 और असम राज्य में 112 मामले दर्ज हैं। इस तरह से ये राज्य सूची में सबसे ऊपर की श्रेणी में मौजूद है। विडंबना यह है कि ये आंकड़े पूरी कहानी को बयाँ नहीं कर सकते हैं। यूएपीए (UAPA) के अलावा, एनआईए (NIA) अधिनियम में 2019 के अंतर्गत हुए संशोधन (जिसके तहत केन्द्रिय एजेंसी दूसरे अपराधों को भी अपनी सूची में शामिल करके अपराधों की जाँच करने के लिए सशक्त बन जाती है) का मतलब है कि यदि हजारों नहीं तो, कम से कम सैकड़ों मामले ऐसे है जहाँ लोगों पर सामान्य आरोप में भी कठोर यूएपीए (UAPA) का क़ानून लगा दिया गया है। संभव यह भी है कि यदि ऐसे राज्य जहाँ यूएपीए (UAPA) की धाराएँ अभी सिर्फ आरोपों में है (यानि कि जिन पर यूएपीए (UAPA) सेक्शन अभी केवल आरोपों में ही है) यदि राज्य ने इन मामलों के बारे में जानकारी साझा नहीं की है तो इसका मतलब है कि वास्तविक यूएपीए (UAPA) मामलों का आंकड़ा उम्मीद से बहुत ज़्यादा हो सकता है।
जहाँ तक कि अब त्रासदी के मानवीय चेहरे का सवाल है। निश्चित रूप से फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत ने देश को झकझोर दिया है, और आज़ादी पर पाबंदी लगाने वाले उन क़ानूनों के ख़िलाफ़ लोगों में गुस्सा पैदा किया है। वह क़ानून जो स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण है, जो पुलिस और कार्यपालिका को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है। हमें धैर्य के साथ इस तरह के क़ानूनों की लंबी परंपरा और दुरुपयोग की सूची को याद करना चाहिए।
16 मई 2014, यह वही दिन है जिस दिन नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में सत्ता में आए थे। ठीक उसी दिन, अहमदाबाद के मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हुसैन मंसूरी सहित छह लोगों को 2002 के अक्षरधाम आतंकी हमले में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया गया था। जबकि 2006 में, इसी मामले में पोटा (POTA) अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। जिसे 2010 में गुजरात उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। ग्यारह साल जेल में बिताने के बाद
आख़िरकार वे बरी हुए लेकिन कैद में उन्हें गुजरात की बदमाश पुलिस के साथ-साथ अन्य लोगों और डी वंजारा द्वारा यातना की क्रूरतम हदों को सहना पड़ा। जेल से बरी होने के बाद, मुफ्ती ने अपने दर्द भरे संस्मरण को ‘ग्यारह साल सलाखों के पीछे : मैं एक मुफ्ती हूं और मैं आतंकवादी नहीं हूं’ को पहले उर्दू और फिर अंग्रेजी में लिखकर दुनिया को बताया।
फैसले पर लिखे गए पैराग्राफ कहते है।
अक्षरधाम फैसला : पैरा. 131 : “…जाँच स्तर से लेकर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने तक, इस मामले के विभिन्न चरणों में विचार करने के दौरान हुई लापरवाही पर ध्यान दें… जब इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों और बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हमारे सामने पेश किया जा रहा हो तो हम शीर्ष अदालत होने के नाते यूँ हीं हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने का जोखिम नहीं ले सकते है।”
पैरा 136 : “फैसले को सुनाने से पहले, हम जाँच एजेंसियों की उस अक्षमता के बारे में अपने दर्द को बताना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने जिस तरह से गंभीर प्रकृति वाले मामले की जाँच घोर लापरवाही के साथ की। जबकि यह एक ऐसा मामला था जिससे राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा जुड़ी हुई थी। कीमती जीवन को तबाह करने के लिए जिम्मेदार असली दोषियों को सजा देने के बजाय, पुलिस ने निर्दोष लोगों को पकड़ा और उनके ख़िलाफ़ गंभीर आरोप लगाए। जिसके चलते उन्हें दोषी ठहराया गया और बाद में सजा सुनाई गई।”
निःसंदेह, इस तरह के फैसले न्यायपालिका के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ाते हैं। हालांकि कहानी में एक क्रूर मोड़ है। इस तरह के आघात और अन्याय की दास्तां की उचित भरपाई की जरूरत होती है। जिसमें अपराधियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलना, दुर्भावना से भरे और ग़लत अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाना शामिल होता है। विडम्बना यह है कि ऐसी जगह पर न्यायपालिका पूर्ण न्याय देने से वंचित रह जाती है। गैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 2004 की धारा 49 की तरह पोटा (POTA) और टाडा (TADA) में भी इसी तरह की धाराएँ है। जिसके तहत अधिकारियों को अच्छे मंशा या अधिनियम के अनुसरण में किए गए कृत्यों के लिए किसी भी अधिकारिक कमेटी, अभियोजन या क़ानूनी कार्यवाही से बचा लेती है! 2004 में सांसदों ने यूएपीए (UAPA) में संशोधन करते हुए एक और कठोर क़ानून को लागू किया। ताकि अपने हाथों में सत्ता लेने वाले और इसका दुरूपयोग की इच्छा रखने वाले अधिकारियों और नौकरशाही के बड़े जनसमूह को प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके।
मुंबई में रहने वाले वाहिद शैख़, जिन पर 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले का ग़लत आरोप लगाया गया था। उन्होंने अभी हाल में 498 पेजों की इनोसेंट प्रिजनर्स (बेगुनाह कैदी) नामक पुस्तक का प्रकाशन किया है। यह एक दस्तावेज है जिससे भारतीय व्यवस्था, अदालतें, क़ानून प्रवर्तन, यहाँ तक कि मीडिया को भी शर्मसार होना चाहिए। हालाँकि अभी तक इस पुस्तक ने ‘मुख्यधारा के लोगों’ पर मुश्किल से ही कोई हलचल पैदा की है। वाहिद को मकोका (MCOCA) के तहत जेल हुई थी। जहाँ उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था और अब वह बरी होकर बाहर आ गए हैं, जबकि उनके साथ जेल में रहे आरोपी साथियों को उम्रकैद और यहाँ तक कि मौत की सजा तक दे दी गई है।
वाहिद शेख, पूर्व में एक स्कूल में शिक्षक रहे थे। इसीलिए शायद उन्होंने अपने हम वतन को क़ानूनी रूप से यातना के बारे में, झूठे आरोपों के बारे में, कैद का सामना करने के बारे में शिक्षा देना ही अपने जीवन का मिशन बना लिया है। यह एक वैकल्पिक आपराधिक न्यायशास्त्र है जिसको एक बार आरोपी रह चुका इंसान, जो खुद उसका शिकार रहा उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस कहानी के और भी जटिल पहलू हैं, उनमें से एक कहानी फादर स्टेन की है। खराब स्वास्थ्य, स्वच्छता और सैनिटेशन की गंभीर स्थिति, एनआईए (NIA) और जेल अधिकारियों दोनों के द्वारा अभद्रता और अदालत के सामने झूठ ने उनके जीवन के आखिरी के दो महीनों को जरूरत से ज़्यादा बदतर बना दिया था। कोविड-19 वायरस से पीड़ित महाराष्ट्र की जेलें भी किसी भी नियमित निगरानी या जाँच से बच जाती हैं। जबकि 2016 में जेल नियमावली और इससे पहले और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसलें सहित अगस्त संशोधन, मजबूत निगरानी तंत्र कि जरूरत पर जोर देते हैं, ताकि विचाराधीन और दोषी कैदियों की उचित गरिमा बनी रहे। ऐसी किसी भी व्यवस्था को पूरी तरह से बंद करने से हमारी जेलें बीमारी, हिंसा और भेदभाव से ग्रस्त हो जाएगी। अगर वास्तव में कोई समाज अपनी जेलों की स्थितियों से मापा जाता, तो भारत एक अंधकार भरा, अपारदर्शी, और बेहद धूमिल तस्वीर पेश करता है।
(लेखिका एक पत्रकार और अधिकार कार्यकर्ता और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की सचिव भी हैं। www.cjp.org.in सीजीपी (CJP) की क़ानूनी शोध टीम और सहयोगी वकीलों ने इस लेख के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं।)